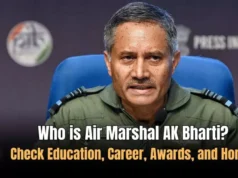महंगे इत्र के शौकीन थे किशन महाराज
दी यंगिस्तान, नई दिल्ली।
पंडित किशन महाराज का जन्म
पं. किशन महाराज का जन्म भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में 3 सितंबर, 1923 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की रात हुआ था। उनके पिता पं. हरि मिश्र कुशल तबला वादक थे। लेकिन उनकी अल्पायु में ही पिताजी का निधन हो जाने के कारण उनके निस्संतान बड़े भाई तालवाद्य शिरोमणि पं. कंठे महाराज ने पुत्रवत् स्नेह देकर उन्हें विधिवत् तबला की शिक्षा दी। उन्होंने ही कृष्ण प्रसाद या किशन प्रसाद को पं. किशन महाराज बनाया।
स्वादिष्ट भोजन, महंगे इत्र के शौकीन
रंगीन और रईस तबीयत के किशन बचपन से ही शानो-शौकत से रहते थे। उत्तम भोजन, सुसज्जित परिधान और बेशकीमती इत्र के शौकीन होने के साथ महिलाओं से मित्रता उनकी हॉबी थी। तबला शिक्षा के प्रारंभिक दौड़ में अर्थात् अभ्यास में वे उतनी रुचि नहीं लेते थे।
संकटमोचन मंदिर में संगीत साधना
किंतु समझदारी विकसित होने के पश्चात् उन्होंने यह महसूस किया कि बनारस में पं. अनोखे लाल और पं. गुदई महाराज ऐसे दो तबला वादक हैं, जिनकी ख्याति बहुत है। साथ ही उस्ताद हबीबुद्दीन खाँ और उस्ताद अल्लारखा जैसे सुयोग्य ताबलिक भी राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहे हैं। प्रतिद्वंद्विता की इस भावना ने किशनजी को कठिन अभ्यास को उत्प्रेरित किया और बनारस के संकटमोचन मंदिर को उन्होंने संगीत का साधना-स्थल बनाया।
पूरी रात मंदिर में करते रियाज
वे सारी रात मंदिर प्रांगण में रियाज करते थे। अभ्यास के क्रम में उनके साथ कई अलौकिक घटनाएँ घटीं, जिसे और इस घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी संगीत-साधना की सफलता का ईश्वरीय वरदान के रूप में मानते थे।

सन् १९४१-४२ में जब उनकी अवस्था अठारह उन्नीस वर्ष की थी तब राजाभाऊ देव की उपस्थिति में आशुतोष भट्टाचार्य के यहाँ कार्यक्रम के दौरान काफी कलाकार एकत्रित हुए। वहाँ तबला वादन के चमत्कारिक प्रसंगों एवं घटनाओं की चर्चाएँ होने लगीं। जहाँ पं. विश्वनाथ मिश्र के गिदीन्न तिहाई की ध्वनि से मोमबत्ती तथा लालटेनों का बुझ जाना, एक सौ बत्तियों के बुझने के साथ छत के पाटन का टूट जाना आदि घटनाओं का वर्णन उपस्थित संगीतज्ञों के द्वारा किया जाने लगा। लोगों का मंतव्य था कि भला ऐसे सिद्ध लोग अब कहाँ हैं! पत्थर तो दूर, शीशा तोड़ने की भी क्षमता अब किसी कलाकार में नहीं है।
किशन जी के गायन ने चटक गया शीशा
यह वाक्य उपस्थित किशन महाराज को आहत किया। तत्क्षण माँ सरस्वती की अर्चना कर तबले पर वे बैठ गए और एक टुकड़ा बजाना शुरू किया। तिहाई के अंतिम ‘धा’ के साथ ही किर्र की तेज आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। जब आवाज की दिशा में लोगों ने मुड़कर देखा तो पाया कि एक कोने में रखी एक अलमारी का शीशा एक छोर से दूसरे छोर तक चिटककर टूट गया। तभी से उन्होंने धोती, कुरता पहनकर और रोली का टीका लगाकर ही वादन करने का निश्चय किया।
पहला सार्वजनिक कार्यक्रम
महाराज जी का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम पं. चतुर्भुज मिश्र उर्फ चौबे महाराज के कथक नृत्य के साथ हुआ था। सन् १९४६ के शुरुआती दिनों में उन्होंने बंबई के लिए प्रस्थान किया। उस समय बंबई में शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गज कलाकारों का जमावड़ा था।
दिल्ली, अजराड़ा, लखनऊ, फर्रुखाबाद और पंजाब घरानों के तबला वादन से तो संगीतज्ञ परिचित थे ही, किंतु किशन महाराज की बनारस की इन सभी घरानों से भिन्न शैली से वे लोग बहुत प्रभावित हुए और यहीं से उनकी ख्याति के मार्ग प्रशस्त होने लगे।
संगीत में प्रयोग का साहस
बंबई में आयोजित एक प्रतिष्ठित संगीत सभा में पं. रविशंकर के साथ बजाने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। बाद में दोनों मित्र बन गए। उनका तबला मात्र रियाजी ही नहीं था बल्कि उसमें सूझ-बूझ, चिंतनशीलता और मौलिकता का भी समावेश था।
जिस काल में पं. गुदई महाराज ने बाएँ की गूँज बढ़ाकर और उसके मुख को विपरीत दिशा में रखकर लोकप्रियता के शीर्ष पायदान की ओर बढ़ रहे थे, जिसका अंधानुकरण अधिकांश तबला वादक कर रहे थे, उसी अवधि में उन्होंने बाएँ को पारंपरिक रूप में ही रखकर उसे और ढीला करके उसकी गूँज को कम करके धारा के विपरीत जाने का दुःसाहस किया, जिसमें वे पूरी तरह सफल हुए।
खयाल एवं ठुमरी के गायन के साथ तंत्र वाह्य और कथक नृत्य की संगति के लिए वे अद्वितीय माने जाते थे। धुपद-धमार की भी उन्होंने जमकर संगत की और स्वतंत्र वादन के क्षेत्र में भी अपना विशिष्ट स्थान बनाया। वे ऐसे चतुर्मुखी वादक थे, जिनसे संगीत की कोई विधा अछूती नहीं रही।
कठिन तालों का सुगमता से वादन
वे उन लोकप्रिय और प्रतिष्ठित कलाकारों में से थे, जिनके साथ एक-एक परंपरा की तीन-तीन पीढ़ियों ने गायन, वादन और नर्तन करके स्वयं को धन्य माना। उनकी रुचि विषम प्रकृति के तालों में अधिक थी, इसलिए तीनताल, झपताल, एकताल, धमार और रूपक जैसी तालों के साथ-साथ वसंत, रुद्र, अष्टमंगल ‘जय, जैत, पंचम’ सवारी, शिखर, मत्त, ब्रह्म, लक्ष्मी एवं गणेश जैसी कठिन और अप्रचलित तालों में भी वे सुगमता वादन करते थे।
भारत के महान संगीतज्ञ
यथानाम तथोगुणः की उक्ति के अनुरूप ही उनका व्यक्तित्व भी था। गौर वर्ण, छरहरा बदन, सुंदर सजीले परिधान, मस्तक पर रोली का विजय तिलक और गले में नवरत्न की स्वर्ण-जड़ित माला पहनकर जब वे मंच पर आते तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हो जाता था।
वे प्रायः शुद्ध बनारसी बाज बजाते थे, लेकिन विभिन्न घरानों की बंदिशों का भी उनके पास संग्रह था वे बहुत अच्छे कवि भी थे युवावस्था में ये ‘मलिक’ उपनाम से हिंदी उर्दू की कविताएँ लिखते थे। संगीत विषय पर उन्होंने अनेक – लेख लिखे हैं। मूर्तिकला एवं चित्रकला में भी वे सिद्धहस्त थे।
इस प्रकार वे संपूर्ण कलाकार थे। किशन महाराज का नाम इसलिए भी आदर के साथ लिया जाता है कि उन्होंने अपनी कला विद्या को अधिक-से-अधिक लोगों तक बिना भेदभाव के पहुँचाया। उनके पुत्र पूरण महाराज स्थापित कलाकार हैं तथा नाती शुभ महाराज युवा तबला वादकों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित किए हुए हैं।
पुरस्कार एवं सम्मान
उन्होंने अपनी युवावस्था में कुछ फिल्मों में भी वादन किया। वे फिल्में हैं- ‘नीचा नगर’, ‘आँधियों’, ‘बड़ी माँ’, ‘पहली नजर’ विश्व संगीत मंच पर धवल कीर्ति पताका फहरा चुके महाराजजी को संगीत सम्राट्, वादन पारंगत, लय भास्कर, संगीत रत्न, ताल चिंतामणि, लय चक्रवर्ती, तबला नवाज, तबला सम्राट्, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान, उस्ताद हाफिज अली खाँ सम्मान, सामापा वितस्ता सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान, स्वरगंगा सम्मान के साथ-साथ काशी विद्यापीठ, जीवाजी विश्वविद्यालय (ग्वालियर), रवींद्र भारती विश्वविद्यालय (कलकत्ता) से डॉक्टरेट की मानद उपाधि एवं ‘पद्मश्री‘, ‘पद्मविभूषण‘ के अलंकरण से सम्मानित किया गया।
निधन
किशन महाराजजी ने अपना जीवन अपने अंदाज में जिया। उन्होंने तीन शादियाँ कीं विख्यात दुमरी गायिका सविता देवी उनकी ही पत्नी हैं। यह महान् कलाकार विशाल शिष्यमंडली के अलावा अपने भरे-पूरे परिवार को त्याग कर ४ मई २००८ की आधी रात के बाद नाद ब्रह्म में लीन हो गया।