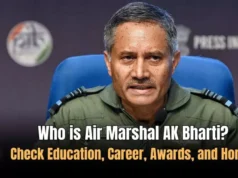विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् समेत विभिन्न अकादमियों की स्थापना की
दी यंगिस्तान, नई दिल्ली।
Maulana Abul Kalam Azad Biography: भारत के देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के आकाश में मौलाना अबुल कलाम आजाद एक ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र थे जिन्होंने अखंड भारत के लिए निरंतर प्रयास किया। मौलाना आजाद ने भारत में धर्मनिरपेक्ष समाज की नींव डालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।
प्रारंभिक जीवन और जन्म, Early Life and Birth
मौलाना खैरूद्दीन तथा बेगम आलिया के परिवार में 11 नवम्बर 1888 को मक्का में जन्में मुहियुद्दीन अहमद अपने जीवनकाल में आगे चलकर मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से जाने गये।
उन्होंने अपने परिवार के साथ कलकत्ता प्रस्थान करने से पहले वर्ष 1897 तक मक्का में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की।
मक्का में उन्होंने कुरान की पढ़ाई पूरी की तथा अरबी, फारसी और उर्दू का प्रारम्भिक ज्ञान भी प्राप्त किया। युवा आजाद को धर्मशास्त्र, विधिशास्त्र तथा दर्शन के प्राचीन साहित्य की शिक्षा भी प्रदान की गयी।
आजाद ने अल्पायु में ही उर्दू समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के लिए कविताएं तथा साहित्यिक और राजनीतिक लेख लिखने शुरू कर दिये।
साहित्यिक लेखन कार्य
बारह वर्ष की आयु में ही वह प्रकाशक बन गये और उन्होंने 1900 में ‘नैरंग-ए-आलम’ नामक एक काव्य पत्रिका निकाली।
सितम्बर 1903 में उन्होंने अपने ही एक अखबार ‘लिसान-अस-सिक’ (सच की आवाज) का प्रकाशन शुरू किया जिसका उद्देश्य सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना, उर्दू का विकास करना तथा साहित्यिक रुचि जागृत करना था।
मौलाना शिवली और सर सैयद अहमद खान की रचनाओं के प्रभाव से उन्हें और प्रेरणा मिली जिसके परिणामस्वरूप भारत को आगे आने वाले समय में सतत् साहित्यिक कृतियां प्राप्त हुई।
ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में सक्रियता
राजनीतिक स्तर पर आजाद के जीवन में पहला बड़ा मोड़ बंगाल के विभाजन के बाद आया जिसे उन्होंने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया।
उसे अस्वीकार करते हुए, आजाद ने स्वयं को ब्रिटिश विरोधी आंदोलन से जोड़ लिया और वह बंगाल विभाजन के परिणामस्वरूप बने कुछ अतिवादी ग्रुपों में शामिल हो गये।
वह देश में उपनिवेश-विरोधी आंदोलन के सभी नेताओं पंजाब में सूफी अंबा प्रसाद एवं अजीत सिंह और अरविंद घोष, श्याम सुंदर चक्रवर्ती तथा लाला हरदयाल के संपर्क में आये।
साप्ताहिक उर्दू अखबार का प्रकाशन
भारत में उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम समुदाय गभीर सैद्धान्तिक संकट के दौर से गुजर रहा था। युवा मौलाना आजाद ने मोहम्मद अली, शौकत अली एवं वजीर हसन जैसे नेताओं तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर ग्रेट ब्रिटेन को एक ऐसी शक्ति माना जो एशिया में इस्लाम का अपमान करने पर तुली हुई थी और जो भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम की आध्यात्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाना चाहती थी।
संकट के इसी समय में आजाद ने जून 1912 से अपना उर्दू साप्ताहिक ‘अल-हिलाल’ शुरू किया। उनका विश्वास था कि उलेमाओं को शिक्षित करने से ही समर्पित तथा आदर्शवादी विशिष्ट वर्ग उभरकर आगे आयेगा जो मुस्लिम समुदाय के नैतिक तथा बौद्धिक पुनरुद्धार के लिए साधन के रूप में कार्य करेगा।
‘अल-हिलाल’ ने मुस्लिम विशिष्ट वर्ग तथा जनसामान्य को राष्ट्रीयता का संदेश दिया तथा उन्हें देश के स्वतंत्रता संग्राम में अन्य समुदायों के साथ शामिल होने की प्रेरणा दी।
अन्याय और दमन के विरुद्ध संघर्ष
वह एक ख्यातिप्राप्त धर्मशास्त्री थे तथा उनकी पत्रिका में इस्लाम के मूल उद्देश्यों की सही व्याख्या राष्ट्रीय दृष्टि से होती थी।
पत्रिका का ऐसा कोई अंक नहीं था जिसमें या तो कुरान की व्याख्या को विस्तारपूर्वक न समझाया गया हो या उन शहीदों की कुर्बानी के बारे में न बताया गया हो जिन्होंने इस्लाम की रक्षा हेतु अपनी जान की बाजी लगायी थी।
अतः ‘अल-हिलाल’ के माध्यम से आजाद ने मुस्लिम समुदाय को बताया कि इस्लाम में व्यक्तिवाद, सामाजिक क्रिया तथा आत्मत्याग के पवित्रतम सिद्धांत हैं। उन्होंने अन्याय और दमन के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने का आह्वान किया।
असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी
मौलाना आजाद की गांधी जी से 18 जनवरी 1920 को हकीम अजमल खां के घर पर लोकमान्य तिलक और अली बंधुओं की मौजूदगी में हुई भेंट का राष्ट्रीय आंदोलन के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। गांधी जी में उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों के लिए संस्थागत समर्थन पाया था।
खिलाफत आंदोलन तथा बाद में असहयोग आंदोलन ने आजाद के राजनीतिक जीवन को एक विशाल मंच प्रदान किया। गांधी जी के हिन्दू-मुस्लिम सहयोग के दृष्टिकोण ने खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया।
मौलाना अबुल कलाम आजाद के राजनैतिक जीवन में एक अन्य मोड़ गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किये गये असहयोग आंदोलन के कारण आया। इसी अवधि के दौरान वह हिन्दुओं और मुसलमानों को एक हो राष्ट्र का अंग मानने लगे।
इस समय तक मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, दोनों के सदस्य थे। परन्तु मुस्लिम लीग द्वारा 1921 में हुए अधिवेशन में ‘सविनय अवज्ञा आन्दोलन’ की निन्दा करने के बाद मौलाना आजाद ने अन्य कई प्रमुख मुस्लिम नेताओं के साथ मुस्लिम लोग को त्याग दिया।
वर्ष 1920 के दशक में हिन्दू-मुस्लिम सहभागिता का समर्थन करने और अधिक-से-अधिक मुसलमानों को काग्रेस में शामिल करने के लिए काफी हद तक आजाद ही उत्तरदायी थे और इस प्रकार उनके प्रयासों से स्वतंत्रता संग्राम ने अधिक जोर पकड़ा। वर्ष 1921 के अन्त में सरकार ने भारतीय नेताओं को अन्धाधुन्ध गिरफ्तार करना आरंभ कर दिया और “कांग्रेस वालन्टियर्स” को एक गैर-कानूनी संगठन घोषित कर दिया।
इससे लोग भड़क गए और उन्होंने सामूहिक गिरफ्तारियां दीं। मौलाना आजाद को 10 दिसम्बर 1921 को कलकत्ता में गिरफ्तार किया गया था।
35 वर्ष की आयु में बने कांग्रेस के अध्यक्ष
वर्ष 1923 में मौलाना आजाद को पैंतीस वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और इस प्रकार वह सबसे कम उम्र के युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने।
इसी अवधि के दौरान मौलाना आजाद पंडित जवाहर लाल नेहरू के संपर्क में आये और उन्होंने उनके साथ ऐसा व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया, जो कि जीवन भर रहा।
ऐसे समय में जब मुस्लिम लीग के नेतृत्व में कुछ लोग विभाजन की मांग कर रहे थे, आजाद इस उपमहाद्वीप की एकता की रक्षा में खड़े हो गए।
1940 में कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष बने
जब कांग्रेस ने 1930 में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, तो आजाद को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने आजादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस द्वारा शुरू की गयी प्रत्येक कार्यवाही में हिस्सा लिया था।
आजाद ने उस समय अपने जीवन का अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य स्वीकार किया जब उन्होंने मार्च 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद पुनः ग्रहण किया क्योंकि यह स्वतंत्रता संग्राम का अत्यंत संकटकालीन दौर था।
करो या मरो का आह्वान
उनकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रसिद्ध ‘भारत छोड़ो संकल्प‘ पारित किया था तथा ‘करो या मरो’ का स्पष्ट आह्वान किया था।
इस आंदोलन को ब्रिटिश सरकार द्वारा बेरहमी से दबा दिया गया तथा मौलाना आजाद को कांग्रेस के शेष नेताओं के साथ गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया।
सत्ता हस्तांतरण में अहम कड़ी
वर्ष 1945 में जेल से रिहाई के बाद उन्हें भारतवासियों को सत्ता के हस्तांतरण के लिए मुस्लिम लीग तथा ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने का अत्यंत नाजुक मामला सौंपा गया।
उन्होंने भारत के वायसराय लार्ड वेवल के साथ बातचीत की। बाद में शिमला में उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लार्ड पैथिक लारेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन के साथ बातचीत के समय कांग्रेस शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।
तथापि, आजाद अशांति के इस दौर में भी अपने शांत स्वभाव और आत्मसंयम के साथ आगे बढ़ते गये, वर्ष 1940 से 1945 के इन ऐतिहासिक छह वर्षों में मौलाना आजाद ने अद्वितीय सम्मान एवं विशिष्टता के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ाया।
जेलों में झेली यातना
मौलाना आजाद एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी एवं महान राजनीतिज्ञ थे। इन सबसे ऊपर नह एक कट्टर देशभक्त थे। यद्यपि ब्रिटिश जेलों में उन्हें कई वर्षों तक कष्ट एवं उत्पीड़न झेलना पड़ा था, परन्तु कोई भी उनकी आत्मा ‘का दमन नहीं कर सका।
जब देश का विभाजन हुआ तो मौलाना आजाद तथा उनके राष्ट्रवादी मुस्लिम अनुयायियों का हृदय टूट गया और अखंड भारत का उनका सपना चूर-चूर हो गया।
उन्होंने अपने को भारतीय एवम् मुस्लिम होने पर गौरवान्वित अनुभव किया, उनके लिए दोनों में कोई भेद नहीं था।
जब जिन्ना के नेतृत्व में लाहौर में पाकिस्तान संकल्प पारित हुआ, तो आजाद ने कहा:
"मैं भारतीय राष्ट्रीयता की अविभाज्य एकता का हिस्सा हूँ। मैं इस महान राष्ट्र के लिए अपरिहार्य हूँ तथा मेरे बिना भारत का यह वैभवशाली स्वरूप अपूर्ण है। मैं भारत का निर्माण करने वाला अपरिहार्य तत्व हूँ। मैं इस दावें से कभी पीछे नहीं हट सकता।"
वास्तव में, वह इस महान राष्ट्र भारत के लिए अपरिहार्य थे।
जब विभाजन के बाद भारत के मुसलमानों ने देश में अपने भविष्य के प्रति गहरी चिंता दिखायी, तो मौलाना आजाद एक राजनीतिज्ञ के रूप में उनके पास गए तथा उनके अन्दर भारतीय होने का विश्वास तथा हिम्मत का संचार करने में उनकी सहायता की।
उन्होंने अपने सहधर्मियों को उन नेताओं के बारे में, जिन्होंने द्वि-राष्ट्र सिद्धांतों का प्रतिपादन करके विध्वंसकारी भूमिका अदा की थी और मिश्रित राष्ट्रीयता के हित को आघात पहुंचाया था, सारण कराते हुए उनसे यह निवेदन किया कि वे फिर से नयी स्थितियों में इस्लामिक दुनिया में एक ‘सम्मानजनक स्थान’ की रचना करें।
भारत के पहले शिक्षा मंत्री
मौलाना आजाद भावनात्मक तथा बौद्धिक रूप से महात्मा गांधी तथा पडित नेहरू दोनों के निकट थे। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह स्वाभाविक था कि वह मंत्रिमंडल में शामिल हों।
स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में वह नेहरू जी के विश्वस्त साथी रहे तथा मंत्रिमंडल में वह उनके निकटतम विश्वसनीय व्यक्ति और सलाहकार थे।
वह 1947 से 1952 तक शिक्षा मंत्री रहे तथा 1952-58 के दौरान शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री रहे। शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना आजाद ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी केन्द्र तथा राज्यों, दानों को है।
देश की शिक्षा प्रणाली तैयार करने में योगदान
स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद देश की शिक्षा प्रणाली को तैयार करने में प्राच्य विद्या के उत्कृष्ट विद्वान के रूप में उनकी क्षमता प्रदर्शित हुई।
उन्होंने 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तथा 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया।। वर्ष 1947 से 1958 के बीच उनकी पहल पर शिक्षा बजट पंद्रह गुणा बढ़ाया गया।
उन्होंने ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की स्थापना की। संगीत, साहित्य और कला का संवर्धन करने के लिए तीनों अकादमियां संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी बनाने का विचार उनका ही था।
उन्होंने भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा भारत में विज्ञान प्रयोगशालाओं की श्रृंखला स्थापित करने में पंडित नेहरू की काफी सहायता भी की।
कई पुस्तकें भी लिखीं
आजाद अभूतपूर्व बौद्धिक तथा मानसिक गुणों से संपन्न थे और अपने लेखों द्वारा ही वह आम लोगों तक पहुंचे थे।
उनकी कुछ उल्लेखनीय साहित्यिक रचनायें हैं: तर्जुमां-अल-कुरान, तजकिरा, गुबार-ए-खातिर और इंडिया विन्स फ्रीडम, उनके द्वारा लिखी गई अंतिम पुस्तक उनकी अपनी आत्मकथा थी।
आजाद के बहुविध लेखों में उनके राष्ट्रवादी दर्शन तथा धर्मनिरपेक्षता पर आधारित धार्मिक दर्शन की झलक मिलती है। वह उन मुस्लिम धर्मोपदेशकों के बीच, जिन्हें वह स्वाभाविक नेता मानते थे, एक ऐसे विद्वान लेखक थे जो अपने लेखों के माध्यम से अपने विचारों को अन्य लोगों तक पहुँचाना चाहते थे।
वह यह भी मानते थे कि शिक्षित वर्ग को पहले जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे आम लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित कर सकें।
तत्व की खोज आजाद का मूल दृष्टिकोण
तत्व की खोज आजाद का मूल दृष्टिकोण था। उनके अनुसार ‘धर्म की एकता एक बड़ा सत्य है जो कि कुरान का मूलभूत आधार है।
कुरान जो कुछ भी प्रस्तुत करता है वह उस पर ही निर्भर रहता है।
उनका यह भी मानना था कि ‘कुरान के किसी अन्य सत्य को इसकी अपेक्षा जानबूझकर उतना नजरअंदाज नहीं किया गया है जितना कि यह’ आजाद का विश्वास था कि सभी धर्मों का उद्देश्य विभाजित लोगों को एक सूत्र में बांधना होता है।
22 फरवरी 1958 को निधन
राष्ट्र ने 22 फरवरी 1958 को इस प्रतिष्ठित विद्वान और दार्शनिक राजनेता के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिसने मानव जाति को एकता की शिक्षा देने का साहस उस समय किया जब कुछ तत्वों ने मनुष्य को मनुष्य से अलग करने के लिए धर्म का सहारा लिया और संकीर्ण राष्ट्रवाद के सिद्धांतों का प्रयोग एक राष्ट्र को अन्य राष्ट्र से अलग करने के लिए किया।
भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था:
"हम आज एक ऐसे महान व्यक्ति के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं जो एक प्रखर बुद्धि वाला और मेधावी व्यक्ति था और जिसमें समस्या की जड़ तक पहुंचने की अद्भुत क्षमता थी। 'प्रखर' शब्द का प्रयोग शायद मैं उनकी बुद्धि की प्रशंसा हेतु सबसे अच्छे शब्द के रूप में कर रहा है। जब हम एक ऐसे साथी, मित्र, सहकर्मी, कामरेड, नेता और शिक्षक से जुदा होते हैं और उनको अपने चीच नहीं पाते हैं तो हमारे जीवन और कार्यों में एक भारी शून्यता आ ही जाती है।"
अपनी प्रतिष्ठित भूमिका में मौलाना आजाद द्वारा दी गई निःस्वार्थ सेवाएं राष्ट्र को सदैव प्रेरणा प्रदान करती रहेगी।
लेटेस्ट पोस्ट
- Tata Punch EV Facelift लॉन्च होते ही मचा हड़कंप! कीमत और रेंज जानकर लोग रह गए हैरान
- Mahindra Thar Highway Viral Video: हवा में उड़कर साइन बोर्ड में घुस गई थार? सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप!
- Volkswagen Tayron R-Line vs Toyota Fortuner vs Jeep Meridian: Big Reveal! नई रिपोर्ट में सामने आया असली पावर किंग, कीमत और फीचर्स ने बढ़ाई टेंशन
- Nissan Gravite vs Renault Triber: 7-सीटर कार में कौन बेहतर? फीचर्स, कीमत में कौन किसपर भारी
- Maruti Suzuki e-Vitara Variant-Wise फीचर्स का बड़ा खुलासा: जानें हर ट्रिम में क्या मिलता है + लॉन्च अपडेट