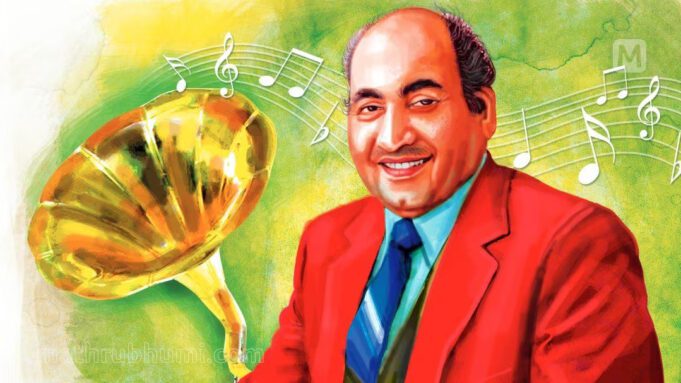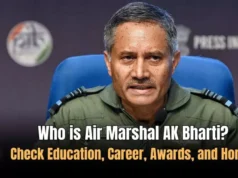रफ़ी साहब: आवाज़, सादगी, और इंसानियत का अनमोल संगम
मोहम्मद रफी जन्म शताब्दी विशेष
लेखक- अरविंद ‘अजल’
“आप मुझे कुछ बना दें।”
अपनी आँखें नीची किए हुए बड़ी ही मासूमियत से एक बेहद सुरीले इन्सान ने अपने सामने बैठे एक शख्स से कहा।
“अरे-अरे, ये आप क्या कह रहे हैं। आप तो बने बनाए हैं। इतनी दौलत, इतनी शोहरत, दुनिया भर में आपके नगमात ब्रॉडकास्ट होते हैं, तो फिर आपको क्या जरूरत है मेरी !”
आश्चर्यजनक भाव चेहरे पर लाते हुए उस शख्स ने कहा।
“नहीं जरूरत है, मुझे आपकी सख्त जरूरत है। आप मेरे गले में मिठास भर दें। मुझे एक नया अंदाज़ दें गाने का।”
उस बेहद सुरीले इन्सान की आवाज में अनुरोध का भाव था।
ये बातें दो अमर शख्सियतें, इस सदी के सर्वकालिक महान गायक रफ़ी साहब और संगीतकार मोहम्मद जहूर ‘खय्याम’ के दरमियान की थीं जिसका जिक्र खय्याम साहब ने बड़े ही भावुक अंदाज में अपने एक साक्षात्कार के दौरान किया था। और फिर इन दोनों महान हस्तियों के बीच महज दो महीने की जुगलबंदी ने वो करिश्मा कर दिखाया कि लोग हतप्रभ रह गए। राग दरबारी के बेहद ऊँचे स्वरों में “ओ दुनिया के रखवाले” को सर्वकालीन अमर गीत बनाने वाले रफी साहब ने जब “तेरे भरोसे हे नन्दलाला”, के साथ पाँच अन्य भजन और “ये न थी हमारी क़िस्मत कि विसाल-ए-यार होता”, के साथ-साथ चन्द दीगर ग़ज़लें बेहद नीचे और मुलायम स्वरों में रिकॉर्ड की तो लोगों के आश्चर्य का तो जैसे ठिकाना ही न रहा।
रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ ही लोगो को इस बात का सुरीला एहसास हुआ कि आवाज़ तीन सप्तक, मन्द्र, मध्य और तार, की भी होती है और किसी भी सप्तक मे गीतों की प्रस्तुति, गायकी के स्तर का बलिदान किए बिना भी, प्रभावपूर्ण ढंग से की जा सकती है और तार सप्तक की ऊंचाईयों पर भी सुर लहरियों के साथ नफासत से खेला भी जा सकता है। एक ही बंदिश में पहाड़ों की ऊँचाईयों पर थिरकती, समंदर की लहरों सी मचलती, किसी नदी की तरह बलखाती, झरनों सी साफ-शफ़्फ़ाफ़ उनकी आवाज़ जब गहरे झील की सी खामोशी इख़्तियार कर लेती थी तो लोगों की तंद्रा अचानक टूट जाती और वे सोचने पर बाध्य हो जाते थे कि क्या वाकई ऐसा संभव था। ‘मन तड़पत हरि दर्शन को आज’, ‘कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो’ जैसी न जाने कितनी ही बंदिशों में ऐसा कमाल कर दिखाया था उन्होंने।
आवाज़ से अभिनय करने की कला या यूँ कहे कि अभिनय को आवाज़ में उतारने में महारत रखने वाले रफ़ी साहब की आवाज़ माहौल वो नज़ाकत के मुताबिक मुखतलिफ अंदाज़ों में ढल जाने का सामर्थ्य रखती थी। फिर वो अंदाज़ चाहे मोहब्बत का हो या दर्द का, ईश्वर की भक्ति का हो या देश भक्ति का, कव्वाली की लरज़िश हो या किसी सूफी का कलाम, शास्त्रीय संगीत के पेंच-ओ-खम हों या गीत वो ग़ज़लों की मुलायमियत, एहसास की जुम्बिश हो या याहू की वहशत वो गर्जना, उनकी आवाज़ गायकी के हर साँचे में ढलकर ऐसा समां बाँधती थी कि सुनने वाला बेसाख्ता दंग रह जाता था हिन्दी फिल्म संगीत के पितामह नौशाद ने 70 के दशक में दिए एक रेडियो इंटरव्यू में कहा था, “मैंने बड़े से बड़े गायक को सुरों से हटते हुए देखा है। एक तन्हा मोहम्मद रफ़ी है जिनको कभी सुरों से हटते हुए नहीं देखा।”
रफ़ी साहब फ़नकार बड़े थे या इन्सान, यह आज तक एक अबूझ पहेली है। पार्श्वगायिका कविता कृष्णामूर्ति ने उनके बारे में अपनी यादें साझा करते हुए कहा कि “मुस्कुराते रफी साहब को प्रत्यक्ष गाते देखना वो सुनना साक्षात ईश्वर को सुनने की अनुभूति देता है। उनके गले में प्योर सिल्क था। सन् 1980 में फिल्म ‘लेडिज टेलर’ के एक दोगाने, जिसमें मुझे भी आख़िर में कुछ पंक्तियाँ गुनगुनानी थी, के आखिरी अंतरे में रफ़ी साहब बार-बार एक शब्द भूल जा रहे थे जिसकी वज़ह से कई री-टेक हुए। रफी साहब भी थक से गए थे । अचानक वो मेरी तरफ घूमे और दोनो हाथों को जोड़ते हुए बड़ी ही मासूमियत से कहा कि ‘माफ करें, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हो रही है। मैं हैरान रह गई। मैं एकदम नई थी, मेरा कोई नाम नहीं था, फिर भी उनका ऐसा व्यवहार! मेरी आँखों से आंसू निकल आए।”
एक और वाक़या भारतीय फिल्म संगीत के रिदम किंग माने जाने वाले संगीतकार ओंकार प्रसाद नैयर से संबंधित है जो अपने संगीत के साथ-साथ अपने समय की पाबंदगी को लेकर भी काफी मशहूर थे। हालांकि रफ़ी साहब भी समय के बहुत पाबंद थे, लेकिन एक बार फिल्म “सावन की घटा” के एक गाने की रिकॉर्डिंग में उन्हें नैयर साहब के पास आने में थोड़ी देर हो गई। आते ही उन्होंने माफ़ी माँगते हुए कहा, “मैं शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में फंस गया था।” नैयर साहब ने रूखे स्वर में जवाब दिया, “आपके पास शंकर जयकिशन के लिए समय था, ओ. पी. नैयर के लिए नहीं। आज से ओ. पी. नैयर के पास भी रफी के लिए समय नहीं रहेगा।” जब पत्रकारों ने हैरानगी जताते हुए रफी साहब से इस वाकये के बारे में पूछा तो रफी साहब ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, “मैं गलत था, नैयर साहब सही थे।” लगभग तीन वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद रफी साहब एक दिन अचानक नैयर साहब के घर चले आए। हतप्रभ नैयर साहब अपने सबसे पसंदीदा गायक को यूँ सामने देखकर अपने जज़्बात पर काबू नहीं रख पाए और उन्हें गले से लगाते हुए कहा, “रफ़ी, यहाँ आकर तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम ओ. पी. से कहीं बेहतर इंसान हो। तुमने अपने अहम पर काबू पा लिया जो मैं नहीं कर सका।”
भाषाई बंदिशो से इतर तक़रीबन सभी भारतीय भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों के साथ-साथ कई विदेशी भाषाओं में भी गाने वाले इस अज़ीमोतरीन गुलुकार ने नामचीन अदाकारों के अलावे कई ऐसे गुमनाम अदाकारों को भी अपनी आवाज़ से नवाज़ा जो आज तक उनकी पहचान बने हुए हैं। फिल्म ‘दोस्ती’ के वो दोनो अनाम कलाकार आज भी महज रफ़ी साहब की बेमिसाल गायकी की बदौलत ही लोगों के दिलों में महफूज हैं। यह उनकी गायकी का ही कमाल था कि किशोर कुमार को भी अपने लिए उनकी आवाज़ लेने को बाध्य होना पड़ा। किशोर कुमार के लिए फिल्म ‘रागिनी’ का गीत ‘मन मोरा बावरा’, फिल्म ‘शरारत’ का ‘अज़ब है दास्ताँ तेरी ऐ ज़िन्दगी’, फिल्म ‘बागी शहजादा’ का ‘मैं इस मासूम चेहरे को अगर छू लूँ तो क्या होगा’ जैसे गीत तो महज़ बानगी हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि उनकी आवाज़ की सीमाएं अनंत थीं। पार्श्व गायक महेन्द्र कपूर ने तो बाक़ायदे उनके नाम का गण्डा बाँध रखा था और उन्हें अपना गुरु मानते थे। ‘तुझे क्या सुनाऊँ मैं दिलरुबा’, ‘मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता’, ‘तकदीर का फ़साना जाकर किसे सुनाएँ’, ‘सुबह न आई शाम न आई’, जैसे कई अमर गीतों के अदाकारों की कभी कोई पहचान नहीं बन पाई, लेकिन उनके लिए गाए रफ़ी साहब के ये गीत कालजयी हो गए।